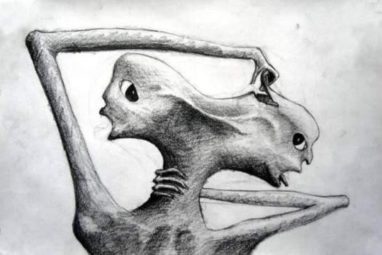साहित्य भी झूठ बोलता है पर उसके सहारे सत्य तक पहुंचता है जबकि सत्ताएं झूठ बोलकर-फैलाकर और बड़े झूठ तक ही हमें ले जाती हैं
अशोक वाजपेयी | 27 जून 2021 | फोटो: रैडिट.कॉम
सत्य की भाषाएं
विश्वविख्यात अंग्रेज़ी साहित्यकार सलमान रश्दी ने 2003-2020 में लिखे निबन्धों के संग्रह ‘लैंगुएजेज़ आव् ट्रुथ’ (हैमिश हेमिलटन पेंमुइन) के बारे में दिये गये एक इण्टरव्यू में कहा कि सत्य की, भारत के समान, अनेक भाषाएं हैं. यह सिर्फ़ भारत को दी गयी एक प्रणति (सम्मान) भर नहीं है. यह इस बात का स्वीकार भी है कि इस तथाकथित ‘सत्यातीत समय’ में सत्य जीवित और सक्रिय है और अनेक भाषाओं में बोला-लिखा-विन्यस्त किया जा रहा है. रश्दी की स्थापना है कि उन्नीसवीं शताब्दी का यथार्थवाद अब पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुका है क्योंकि आज यथार्थ के बारे में कोई व्यापक मतैक्य नहीं है. आज का यथार्थ अतियथार्थ है और उसे विन्यस्त करने के पुराने ढांचे बेकार हो चुके हैं. सत्य मानों यथार्थ का मामला इतना नहीं रह गया है जितना कल्पना का. यथार्थ तो अभूतपूर्व रूप से विखण्डित है, टूटा-बिखरा हुआ और उसे कल्पसृष्टि ही एकत्र कर सकती है, यथार्थवादी युक्तियां नहीं.

रश्दी अब अधिक मुखर ढंग से यह स्वीकार कर रहे हैं कि सत्य की कोई एक प्रामाणिक भाषा नहीं है: भाषाएं भी कई हैं और उनमें चरितार्थ होने वाले सत्य भी. सत्य की बहुलता अनिवार्यतः भाषाओं की बहुलता में प्रतिफलित हो रही है. यह कठिन कर्म है क्योंकि सचाई के बजाय झूठ को फैलाने-प्रतिष्ठित करने के अपार साधन हैं और ऐसे उपक्रम अब विश्वव्यापी हैं. सच के बजाय झूठ को फैलने के अधिक तत्पर अवसर हैं. जब किसी समाज का या कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा झूठ में विश्वास करने लगे और उसकी प्यास, और झूठ की प्यास, एक हो गयी हो तो साहित्य अनिवार्यतः एक अल्पसंख्यक कर्म हो जाता है. साहित्य भी गल्प रचता है, झूठ बोलता है पर उसके सहारे सत्य तक पहुंचता है जबकि सत्ताएं झूठ बोलकर-फैलाकर और बड़े झूठ तक ही हमें ले जाती हैं. ऐसा न सिर्फ़ अमरीका में हुआ है, हो रहा है, भारत में भी स्थिति उतनी ही ख़राब है. झूठ का बोलबाला है और सच का मुंह लगभग काला किया जा रहा है. रश्दी को इसका तीख़ा अहसास है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो उलटी दुनिया है, ‘जहां पागलखाना पागल चला रहे हैं’. वे उनके साथ हैं और उनके प्रशंसक हैं जो सच को सच मानते हैं और झूठ को झूठ कहने का जोखिम उठाते हैं. उनका इसरार है कि राजा अगर नंगा है तो उसे नंगा कहने की भाषा सत्य की भाषा है. वे उस जादू में विश्वास करते हैं जो सत्य की भाषाओं से सम्भव होता है और चाहते हैं कि हम यक़ीन करें कि अन्त में सत्य हमें मुक्ति देगा.
‘इसके पहले कि पुस्तकें हों, कहानियां थीं. पहले वे लिखी नहीं जाती थी. कभी-कभार उन्हें गाया जाता है.’ रश्दी की पुस्तक का आरम्भ इन वाक्यों से होता है. वे आगे कहते हैं कि गल्प का जन्म आश्चर्य कथाओं से हुआ. उनकी विस्मयकारी सुन्दरता इस बात से निकलती थी कि हम एक साथ यह जानते थे कि कहानी कल्पना से जन्मी है याने कि अयथार्थ है और यक़ीन करते थे कि उसमें कोई गम्भीर सच है.
बिन पानी सब सून
गरमी के दिन हैं और प्यास बहुत लगती है इसलिए पानी पर ज़्यादा ध्यान जाता है. पर पानी को लेकर एक विश्वव्यापी संकट है जो गहराता जा रहा है. हमारे दिवंगत मित्र अनुपम मिश्र ने हमें पानी बचाने के लिए तरह-तरह से आगाह किया और यह भी बताया कि साफ़ माथा रखने-वाला समाज पानी की चिन्ता करता है और उसके संरक्षण के सामुदायिक तरीकों की ईजाद और पालन भी. आम तौर पर, भारतीय धनाढ्य और मध्य वर्ग पानी की ख़ासी बरबादी करते रहते हैं, बिना इसकी परवाह किये कि दुनिया में पानी लगातार कम हो रहा है और उसे किफ़ायत से बरतने की ज़रूत है. रंगहीन, स्वादहीन, गन्धहीन, चिर नवीन पानी संसार की सबसे सादी और जटिल चीज़ है. मानवीय अस्तित्व काफ़ी हद तक उस पर निर्भर है और उसकी बढ़ती तंगी के चलते यह भविष्यवाणी तक की गयी है कि अगला विश्वयुद्ध पानी को लेकर होगा. रूपर्ट राइट ने अपनी 2008 में प्रकाशित पुस्तक ‘टेक मी टू द सोर्स: इन सर्च आव् वाटर’ में कहा है कि ‘भारत सरकार चन्द्रमा पर यान भेजने में अधिक व्यस्त है न कि दिल्ली में पाइपों में पानी भेजने में. दुनिया जलवायु से अधिक आक्रान्त है बजाय इसकी चिन्ता करने के कि एक अरब लोगों को साफ़ पानी नहीं मिलता है. पानी में कोई वोट नहीं मिलते.’ राइट यह भी बताते हैं कि पानी को समय मिले तो वह सबसे सख़्त चट्टान को भेद सकता है. अगर पर्याप्त मात्रा में हो तो वह आग बुझा सकता है, पहाड़ों का हिला सकता है और सब कुछ को नष्ट कर सकता है. लोगों की तरह पानी सबसे प्रसन्न होता है जब वह गतिशील होता है. हमारे प्रिय कवि रघुवीर सहाय ने यों ही नहीं कहा था: ‘मन में पानी के अनेक संस्मरण हैं.’
इतना कितना जीवन
यह प्रश्न आज तक खुला हुआ है कि कोई भी लेखक अपना कितना जीवन अपने साहित्य में डाल पाता है. प्रश्न तो यह भी उठता रहा है कि क्या लेखक अपना जीवन ऐसे डालना चाहता भी है? और यह भी कि ऐसा कर पाने की सर्जनात्मक क्षमता क्या हर लेखक में होती है? एक उपप्रश्न यह बनता है कि क्या पाठक की ऐसी कोई अपेक्षा होती है कि वह किसी कृति के माध्यम से उसके कृतिकार के जीवन को जाने-समझे?
यह तो निर्विवाद है कि साहित्य से जीवन कहीं अधिक बड़ा, व्यापक और विपुल होता है, लेखक का जीवन भी और व्यापक जीवन भी. समूचे जीवन को उसके सभी रगों-रेशों को साहित्य में ला सकना लगभग असम्भव है. जीवन है ही ऐसा कि वह किसी एक माध्यम में, जैसे कि साहित्य में, समा ही नहीं सकता. जो भी जीवन साहित्य में याने भाषा के दरवाज़े से जाता है उसमें परिष्कार, संक्षेप आदि अपने आप होते जाते हैं और इस प्रक्रिया में वह बदल जाता है. साहित्य लगभग ज़रूरी तौर पर जीवन को बदल देता है: रचना में यथार्थ के अलावा स्मृति और कल्पना का अनिवार्य रसायन होता है. रचना में लेखक के अपने जीवन के अलावा अन्य जीवन भी प्रवेश कर जाते हैं. फिर भाषा का रूपकों-बिम्बों-अन्तर्ध्वनियों आदि का अपना जीवन होता है जो कृति में अपनी जगह बना लेता है. इस तरह कृति में जो जीवन चरितार्थ होता है वह लेखक के जीवन से अलग हो जाता है. ऐसे अवसर आते हैं जब लेखक अपने किन्हीं जीवन-प्रसंगों को उनके दुखते मूलों से त्रस्त होकर उनके आशय और फलितार्थ बदल देता है और कई बार जो जीवन में नहीं कर पाया वह कृति में कर डालता है. इतना तो हर समय स्पष्ट रहता है कि साहित्य और जीवन का सम्बन्ध ख़ासा जटिल और गतिशील होता है.
अकसर यह समझा जाता है कि किसी भी लेखक का साहित्य उसकी आत्मकथा भी होता है. कथाकारों के यहां विशेषतः किसी चरित्र को लेकर यह कल्पना की जाती है कि वह लेखक स्वयं है. सही है कि साहित्य में लेखक के आत्म का निवेश होता है पर ऐसा बहुत सारा है उसी आत्म का जो या तो छूट जाता है या जिसे लेखक अपनी रचना के लिए आवश्यक नहीं समझता. उसमें जो ‘पर’ होता है वह भी कई बार अप्रत्याशित रूप से लिखते समय आता है जबकि लेखक के वास्तविक जीवन में वह या तो था ही नहीं या वैसा नहीं था. घटनाएं, प्रसंग, विचार, स्मृतियां, व्यक्ति आदि वास्तविक जीवन से उठाये जाकर जब किसी कृति में आते हैं तब अकसर वे बदल जाते हैं. यह भी हो सकता है कि लेखक अपनी रचना में अपने जीवन का प्रतिलोम खोजे-गढ़े. जैसे जीवन में, वैसे ही साहित्य में अनेक सम्भावनाएं होती हैं. किसी लेखक ने अपने जीवन में जो सम्भावना चुन, हो सकता है वह साहित्य में उससे किसी अलग सम्भावना का सन्धान करे. साहित्य लेखक का प्रायः दूसरा जीवन होता है, ऐसा जीवन जो उसके वास्तविक जीवन को भी और भरा-पूरा, और अर्थवान् करता है.
>> सत्याग्रह को ईमेल या व्हाट्सएप पर प्राप्त करें
>> अपनी राय mailus@en.satyagrah.com पर भेजें